सूर्य:समय का खेल
भोर
बिल्ली की तरह
दबक–दबक कर आती है,
चुपचाप,
नाखून छिपाए हुए।
दोपहर
बाघ की तरह
अपनी अयाल झटकती है,
धूप के पंजे फैलाकर
धरती पर गुर्राती है।
छायाएँ सिमटती हैं,
पसीना भाषा बन जाता है,
और पल
आग की लकीरों में
गलते जाते हैं।
शाम
चूहे की तरह
सहमी–सहमी,
घबराई हुई
सुराख़ ढूँढती है।
दिन
खेल की तरह
खर्च हो जाता है,
हँसी में,
थकान में,
भागदौड़ में।
और सूर्य—
समय की देह में छिपा हुआ
एक निपुण खिलाड़ी,
हर चाल में
हमें चलाता हुआ।
रात के आते ही
वह मुस्कराता है—
कल फिर
यही खेल
नए रूप में खेलेगा।"
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
विज्ञापन

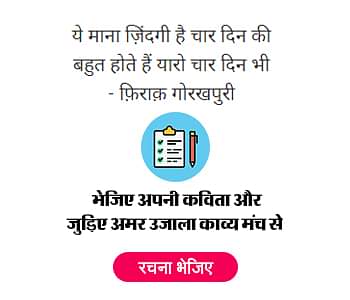






कमेंट
कमेंट X