पहले बता, तू कौन है
पहलगाम की घाटी में
न तिनका हिला, न पत्ता बोला,
पर वर्दी में लिपटे कुछ सपूत
धूप से पहले ही सो गए थे अकेला।
आतंक की आँखें थीं बेआवाज़,
पर सवाल तेज़ थे, जैसे छुरियाँ—
"तेरा नाम क्या है? धर्म क्या है?
किस ख़ुदा के लिए तू साँसें लेता है?"
एक ने कांपती आवाज़ में कहा—
"मैं उस धरती का बेटा हूँ
जहाँ शिव भी बसते हैं,
जहाँ मस्जिद की अज़ान में
घंटी की गूंज भी हँसती है।"
पर वो न समझे, न रुके।
उन्हें मतलब नहीं था देशभक्ति से,
न ही उस माँ से
जिसकी कोख ने उसे वर्दी पहनाई थी।
उन्होंने देखा उसके नाम की पट्टी,
और लहू की स्याही में
एक मज़हब लिख डाला।
कभी किसी ने 'इमरान' से पूछा,
कभी 'राजेश' से,
"क्या तुम हमारे नहीं हो?"
जैसे देश की मिट्टी ने
हर जन्म से पहले
काग़ज़ भरवाया हो।
क्या अब शहीद होने से पहले
सरनेम बताना होगा?
क्या कफन बाँटने से पहले
मज़हब की मोहर लगेगी?
घाटी अब भी चुप है—
लेकिन वो पेड़, जिन पर खून टपका था,
अब भी सरसराते हैं
हर झोंके में पूछते हैं—
"वो कौन था?
और क्या वाक़ई
ये जानना ज़रूरी था?"
मरना आसान होता अगर
पहले ये साबित न करना पड़ता—
कि मैं ‘इंसान’ हूँ,
फिर ‘हिंदू’ या ‘मुसलमान’..."
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
विज्ञापन

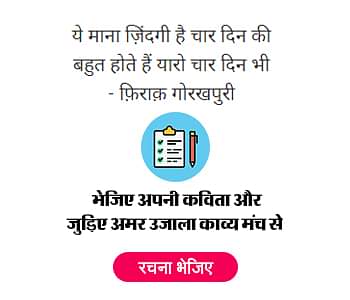






कमेंट
कमेंट X