कुछ दिन की छुट्टी चाहिए... :
हर रोज़ की दौड़ थकाने लगी है,
ये Metro भी अब सताने लगी है।
ना नींदें रही हैं, न सपने वही हैं,
ज़िंदगी हमें आजमाने लगी है।
वो खिड़की के कोने का शांत सा मंज़र,
अब आँखों में धुँधलाने लगी है।
हर चेहरा उदासी का मासूम लिबास,
मुस्कान भी अब तो छुपाने लगी है।
न मीटिंग का मतलब, न ईमेल की भूख,
ये दौड़ हमें खा जाने लगी है।
बस चाह है — कुछ दिन सुकूँ में रहें हम,
जहाँ रूह भी मुस्कुराने लगी है।
ना वक़्त की पाबंदी, ना शोर का बोझ,
जहाँ चाय भी गीत गाने लगी है।
मैं अंकित पंडित, थक गया हूँ बेहद,
अब साँसें भी जैसे बोझ बनने लगी है।
- अंकित पंडित
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
विज्ञापन

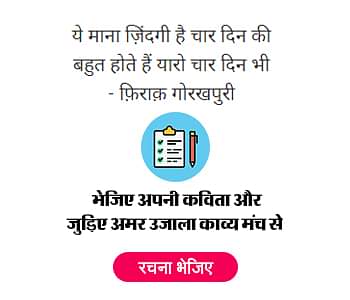






कमेंट
कमेंट X