वो जीवित है, पर जीवंत नहीं
मैंने उनको देखा
अपने घर के आँगन में।
वो जीवित है,
पर जीवंत नहीं।
ना खुलकर कभी वो हँसती है,
ना ही मैंने रोते देखा।
हर क्षण उनको
बस मैंने
औरों की फ़िक्र में
तपते देखा।
वो टूट चुकी है
अंदर ही —
ख़ुद को ढूँढ़
ना पाती
ख़ुद में ही।
वो न जाने
क्या खाती है;
थाली में
बस ताने
और धिक्कार दिखे।
किस-किस की पसंद बनाती है,
नाना पकवान खिलाती है।
वो भूल गई क्या
प्रिय उनको —
मुख पर
श्रृंगार सजाती है?
किन वस्त्रों में
वो सजती हैं,
क्या उत्तम
उनको लगता है —
न जाने
क्या-क्या सहती हैं,
मस्तक पर
शिकन न लाती हैं।
विसार दिया
ख़ुद को ही —
क्या पाने की
वो इच्छुक हैं?
ख़ुद से क्या
वैराग्य लिया;
या ईश्वर की
वो मूरत हैं?
झोंक दिया
अपना सब कुछ ही
इस गृहस्थ
होम के मंडप में।
सर्वस्व त्याग —
एक स्त्री, पत्नी;
और व्यर्थ ही
मात बनी।।
स्वयं हीन होकर
क्या पाया?
क्या पाया
इन बलिदानों से?
ना जीवन में
सम्मान मिला,
ना मिला
स्वयं का अस्तित्व ही।
जिनकी ख़ातिर
सब लुटा दिया,
क्या पूर्ति करेंगे
इस जीवन की?
तुम अथाह
प्रेम का सागर हो;
ऐसे ना
ख़ुद को हीन करो।
सींचो इस जग को
ममता से,
पर ख़ुद का भी
कुछ ध्यान धरो।
जो आए
आँच अस्तित्व पर तेरे —
मर्दन करके
बहिष्कार करो।
तुम ख़ुद का भी
सम्मान करो..खुद का भी सम्मान करो।।
- प्रियांशी सिंह
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
विज्ञापन

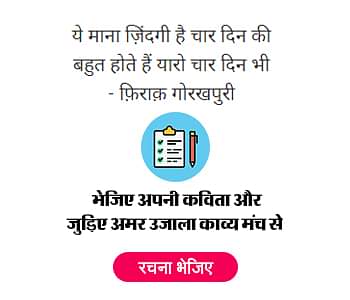






कमेंट
कमेंट X