सर्वेश्वरदयाल सक्सेना: आ गई मुझको स्वयं की याद, फिर, बहुत दिन बाद

फिर बहुत दिन बाद—
सामने की रेंड़ चुटकी,
हिला सरपत का भुआ,
डुगडुगी नीलाम-घर की
चुप हुई,सिर उठाकर किसी मँगते ने
मुझे दी दुआ।
आ गई मुझको स्वयं की याद,
फिर, बहुत दिन बाद।
छोड़कर अपना कृत्रिम यह साथ.
मुड़ चला मैं स्वयं में मिलने;
घने कुहरे से ढँकी
वीरान वादी में
दबे पैरों आ गया मैं,
रुँधे बाड़े तोड़कर
शक्ति-भर मैंने पुकारा :
कोटरो में फड़फड़ाए पंख,
अँधेरी छाया लगी हिलने,
लड़खड़ाने लगी मेरी साँस,
सिर झुका, संध्या लगी फिरने,
‘मैं नहीं हूँ शेष’—
अरा अरा कर चेतना की डाल टूटी,
‘नहीं, अब नहीं मैं रहा’—
चीख़ कर मुख ढाँप छायाएँ गिरीं।
तभी चरमराए द्वार—
अंधगृह-वासी,
मौन संन्यासी,
बढ़ा बाँहें खोल,
शून्य टटोल-टटोल,
काँपते स्वर में लगा कहने—
रुका जल जैसे लगा बहने :
‘आ गए तुम :
कभी आओगे
बस इसी विश्वास पर
डाल से था टँका पीला पात।
सुनो, अब जिया जाता नहीं,
नित्य के इस स्वाँग से
मैं थक गया हूँ,
हो सके तो बस करो;
साँस मेरी घुट रही है
कहो तो चेहरे लगना छोड़ दूँ,
अभी कब तक चलेगा अभिनय तुम्हारा?
हमारी लाश को भी
नाटकी पोशाक पहनाकर नचाओगे?
बुरा मत मानो—
मैं नहीं कहता कि जीवन मत जियो,
सभी जीते हैं,
तुम्हें भी पड़ेगा जीना
जानता हूँ,
किंतु कुछ ऐसा करो,
पैर रखने की जगह हो तो,
एक अंगुल भूमि भी ऐसी मिले
जहाँ मैं जो हूँ
वही बनकर खड़ा रह सकूँ,
सिर उठाऊँ,
एक क्षण को ही सही—
सत्य जो समझूँ
उसे देखूँ, सुनूँ, कह सकूँ।
‘बात क्या मैंने बड़ी कह दी?
आज इतना भी असंभव है?
दूसरो की दृष्टि से ही
तुम्हें ख़ुद को देखना
इतना ज़रूरी है?
मैं नहीं कुछ रहा?
इसलिए मैं पूछता हूँ यह
कि शायद ज्ञात तुमको
यह न हो—
मैं आज अंधा हूँ—
क्योंकि तुम,
सदा अनदेखी कराते रहे;
मैं आज बहरा हूँ—
क्योंकि तुम
अनसुनी करता हूँ इसके लिए
मजबूर करते है;
और अब—
पैरों तले का साँप तक
मुझको दिखाई नहीं देता,
मरण-शय्या की पुकारें,
अनाथों की चीख,
लावरिस कराहें
कुछ सुनाई नहीं देतीं।
अब यहाँ रहना न रहने की तरह है।
इधर देखो
डाल का यह टँका पीला पात
हवा लगाकर
खड़खड़ाता है—
मैं तो मनुज हूँ।
क्षमा कर देना मुझे,
मैं नहीं यह लहू मेरा बोलता है,
क्योंकि तुम
होंठ मेरे सिल चुके हो,
और अंत:करण की आवाज़ तक
गिरवी रख आए हो।
क्या करूँ?
ठठरियों में साँस है जब तक—
कहीं से आवाज़ आएगी,
तुम न जागो, तुम्हारी मर्ज़ी,
किंतु यह तुमको जगाएगी;
और जिस दिन
इसे बेचोगे,
मैं नहीं हूँगा—
और तुम भी रहोगे? शायद!’
इसे सुनकर
झुकाकर सिर
मैं चला आया,
दीप जैसे
स्वयं अपनी ही समाधि
पर जला आया;
इसी बुझी वीरान वादी में—
“सभ्य हूँ मै :
ज़माना जैसा बनाएगा बनूँगा,
...कहाँ जाऊँ?”
पर न जाने क्यों
बोल मैं पाया नहीं,
गला मेरा रुँध गया :
छा गया बेहद घना अवसाद—
फिर बहुत दिन बाद।

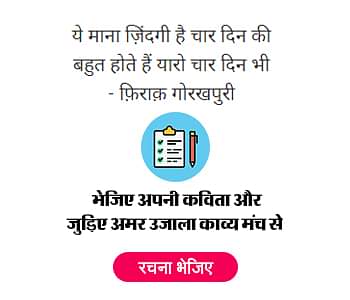






कमेंट
कमेंट X