रवायत के प्रति रुमान तो इतना कि ग़ालिब और दाग़ के मिसरे भी फ़ैज के यहां मिलते हैं...

फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जब यह कहते हैं कि ‘मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे मेहबूब न मांग’ तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वह शख़्स कौन है, जो अपनी महबूबा को अपनी मजबूरी बताते हुए कह रहा है,
लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजै
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजै
क्या यह सिर्फ़ फ़ैज अहमद फ़ैज की आवाज़ है? क्या यह सिर्फ़ उन्हीं का ख़्याल या नज़रिया है? शायद नहीं। यह आवाज़ संभवतः हमारे युगबोध की आवाज़ है, हमारे समय की सच्चाईयों और बदलते ज़रुरत की आवाज़ है। यह वह आवाज़ है जो साहित्य के मयारों को बदलने की बात करती है, उसके उद्देश्यों को बड़ा करके देखने की माँग करती है। लेकिन यह बदलाव इतना अचानक और आक्रामक भी नहीं है कि समूची परम्परा से हमारा नाता ही टूट जाए, बल्कि इसमें पुराने के स्वीकार के साथ उसे नया करने का इसरार है।
आगे पढ़ें
विज्ञापन

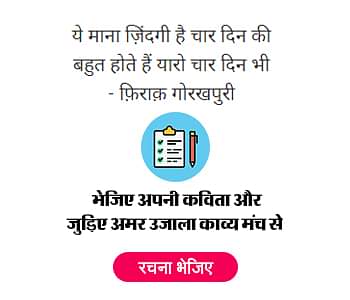






कमेंट
कमेंट X