हिंदी दिवस 2023: भाषा सिर्फ़ संचार का माध्यम ही नहीं अपितु वह संस्कृति की वाहक भी होती है

किसी भी नए काम के शुरुआत के लिए अमृत काल सबसे सही समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमृत काल वही समय है जब बड़ी से बड़ी उपलब्धि को भी हासिल किया जा सकता है । आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या हमने हिंदी के क्षेत्र में भी इतना कुछ प्राप्त कर लिया है कि हम महोत्सव मना सकें ? क्या हम उस अमृत काल में पहुँच गए हैं जहां से हिन्दी उत्थान के लिए उठाए जा रहे प्रत्येक कदम आवश्यक रूप से शुभ और सफल ही होंगे ?
आज़ादी पूर्व: हिंदी का राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान
आज़ादी के आंदोलन में सभी भारतीयों को एक सूत्र में बाँधने वाली तमाम कारकों में हिंदुस्तानी भाषा एक प्रमुख कारक थी । तमाम अहिंदी क्षेत्र के जन नायकों ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी बताया । महात्मा गांधी , लोकमान्य तिलक , राजागोपाल चारी , काका कालेलकर , केशव चंद्र सेन आदि प्रमुख नाम है । काका कालेलकर के शब्दों में , ‘यदि भारत में प्रजा का राज चलाना है , तो वहाँ की जनता की भाषा में चलाना होगा ।’ लेकिन आज़ादी के बाद की जनता की भाषा की स्थिति किसी से छुपी नहीं है।
आज़ादी के बाद हिन्दी
अपने ही घर में दोयम दर्ज़े के नागरिक के तौर पर रहने के लिए अभिशप्त हिन्दी की संवैधानिक स्थिति ऐसी नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इसे राजभाषा का पद दिया है ( अनुच्छेद 343 (1) )। इसका अर्थ है है कि केंद्र अपने सारे कार्यकाज और राज्यों से शासकीय संचार हिन्दी भाषा में ही करेगा। साथ में एक शर्त थी कि अंग्रेजी का प्रयोग आगे के 15 वर्षों तक बना रहेगा। अंग्रेजी के प्रयोग को कम करने और उसी के समान्तर हिन्दी का प्रसार हो ; इसके लिए भारत के संविधान भाग 17 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया विशेष निर्देश इस प्रकार है :- "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों के का माध्यम बन सकें तथा उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वाँछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी करे। "
अंग्रेजी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद भी नौकरशाही और शासन अभिजात्य और आधिपत्यवाद के संस्कारों से मुक्त नहीं हुआ। अंग्रेजी के प्रयोग को कम करने की ज़िम्मेदारी जिन नौकरशाहों को दी गयी , वो कर्तव्यच्युत रहे। इन पंद्रह सालों में हिन्दी के प्रयोग में कुछ ख़ास वृद्धि नहीं हुई। अंग्रेज़ी एक भाषा की जगह श्रेष्ठता की पहचान बनायी गयी। सदियों की गुलामी ने हमारे मेधा शक्ति को ऐसा आच्छादित किया कि हमने अंग्रेजी को मालिक और अपनी हिन्दी को नौकर समझ लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब अंग्रेजी को पूरी तरीके से अपदस्थ करने का समय आया तो उपनिवेशवादी अंग्रेजी तंत्र ने संकीर्ण क्षेत्रीय शक्तियों से हाथ मिलाकर हिन्दी के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया कि संसद को राजभाषा अधिनियम 1963 पास करना पड़ा जिसमें प्रावधान था कि अंग्रेजी का प्रयोग तब तक बना रहेगा जब तक संसद कोई और कानून नहीं बना देती ! अब हिन्दी विरोधियों को संसद के इस कानून का सहारा मिल गया जिसे प्रयोग करके हिन्दी के विरुद्ध और माहौल बनाया जाने लगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन राज्यों यथा तमिलनाडु , आंध्र प्रदेश , बंगाल , महाराष्ट्र आदि से हिन्दी को सबसे ज़्यादा समर्थन दिया और इसे देश को जोड़ने वाली भाषा कहा , उन्हीं राज्यों में हिन्दी के बहिष्कार के लिए आंदोलन होने लगा। इसका कारण राजनीतिक था।
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने देश को तीन समूहों में वर्गीकृत किया है : क ,ख और ग क्षेत्र। ये राज्य समूह हिन्दी के प्रयोग की मात्रा के आधार तय किये गए हैं। क राज्यों के सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों में अधिकतर कार्य हिन्दी में किये जाते हैं। ख और ग क्षेत्रों में प्रयोग क्रमशः कम से कमतर है। सबसे बड़ी चुनौती ग समूह के क्षेत्रों में है जहाँ हिन्दी का प्रयोग न्यूनतम है। इस श्रेणी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश (तेलंगाना समेत)। इन राज्यों के नेताओं का आरोप है कि हिन्दी हमारी मातृ भाषाओं को ख़त्म कर सकती है। यह अपने मूल में साम्राज्यवादी है।
हिन्दी कोई बाहरी भाषा नहीं कि उसे अपने ही देश में उपनिवेश स्थापित करना पड़े। यह तो देश के बहुलांश द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। हिन्दी का अन्य बोलियों से बहनों का है , माँ और बेटी का नहीं ; और सभी बहनों की माँ है संस्कृत।
हिन्दी के प्रयोग का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना है बल्कि कार्यालयीय सम्पर्क भाषा के रूप में आज जिस अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है उसकी जगह राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करना है। साफ है कि हिन्दी अपने मूल में साम्राज्यवादी बिल्कुल भी नहीं है। भाषा सिर्फ़ संचार का माध्यम ही नहीं अपितु वह संस्कृति की वाहक भी होती है। विदेशी भाषा अंग्रेजी ने जिस तरीके से आधुनिकरण के नाम पर पश्चिमीकरण कर डाला , उससे भारतीय संस्कृति दूषित होने लगी। संस्कृति के इस आदान प्रदान में फ़ायदा कम दूषण ज़्यादा हुआ।
आगे पढ़ें
विज्ञापन

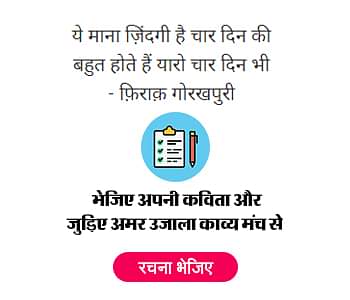






कमेंट
कमेंट X