Shiv Sena Crises: क्या जयललिता दांव से पार्टी बचाएंगे उद्धव, जानें शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई में आगे क्या-क्या होगा?
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
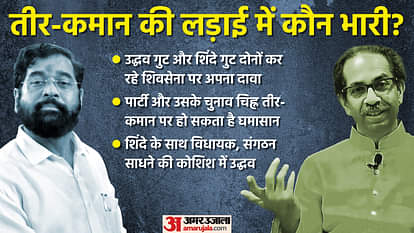
विस्तार
महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है। एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने हैं। इस बीच शिवसेना के बागी गुट से 13 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की खबरें हैं। उधर, बागी गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है। दूसरी ओर अपने इस्तीफे का एलान करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे पास शिवसेना है और उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ऐसे में सवाल है कि शिवसेना किसके पास जाएगी? तीर-कमान चुनाव चिह्न किसके पास जाएगा? ये लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है? भारतीय राजनीति के पुराने उदाहरण क्या कहते हैं? कौन से उदाहरण हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए उम्मीद जगाते हैं? कौन से उदाहरण हैं जिनसे बागी गुट का पलड़ा भारी है? आइए जानते हैं…
भारतीय राजनीति के पुराने उदाहरण क्या कहते हैं?
पार्टियों में इस तरह की लड़ाई के कई उदाहरण हैं। कभी लड़ाई कुछ महीने में खत्म हो गई तो कभी ये वर्षों चली। कभी चुनाव आयोग ने बागी गुट को असली पार्टी माना। कभी बागी गुट को पार्टी और सिंबल दिया। कभी दोनों गुटों को नया सिंबल मिला।
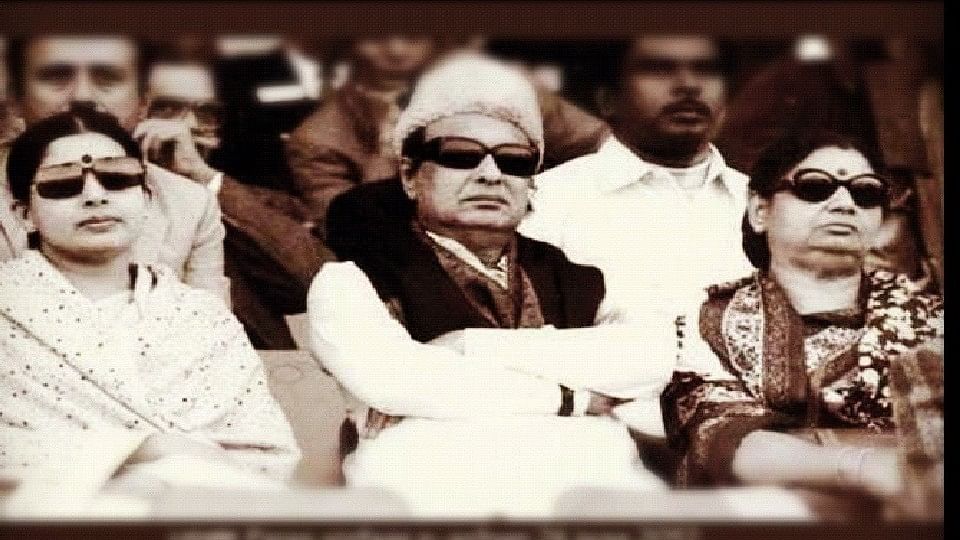
कौन से उदाहरण हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए उम्मीद जताते हैं?
उद्धव ठाकरे को जिस मामले से सबसे ज्यादा उम्मीद है वो जयललिता का मामला। पार्टी जब से बगावत हुई तभी से उद्धव और आदित्य ठाकरे लगातार पार्टी के अलग-अलग संगठनों के साथ बैठकें कर रहे हैं। आइए जयललिता के मामले से समझते हैं कि आखिर उद्धव किस तरह शिवसेना पर अपना दावा मजबूत कर सकते हैं।
बात 1987 की है। उस वक्त तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सत्ता में थी। एमजी रामचंद्रन मुख्यमंत्री थे। 24 दिसंबर 1987 को रामचंद्रन का निधन हो गया। उनके निधन के साथ एआईएडीएमके के दो गुटों में पार्टी पर नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो गया। एक गुट की अगुआई एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन कर रही थीं। वहीं, दूसरे गुट की अगुआई पार्टी की सचिव जयललिता कर रही थीं।
पार्टी के धड़े ने जानकी को पार्टी महासचिव चुन लिया तो जयललिता धड़े ने कार्यकारी मुख्यमंत्री नेदुनचेहिन को पार्टी का महासचिव चुन लिया। दोनों गुटों की ओर से एक-दूसरे पर पुलिस केस तक हुए। दोनों धड़ों ने राज्यपाल के सामने अपने-अपने दावे पेश किए। राज्यपाल ने जानकी रामचंद्रन को सरकार बनाने का न्योता दिया। क्योंकि उस वक्त ज्यादातर विधायक जानकी के साथ थे। जानकी को 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था। वहीं, जयललिता के पास केवल 30 विधायकों का समर्थन था।
28 जनवरी 1988 को जब जानकी सरकार को सदन में बहुमत साबित करना था। उस दिन विधानसभा में जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने सदन के अंदर लाठीचार्ज तक किया। नतीजा ये रहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। तीन हफ्ते पुरानी जानकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया।
इसके बाद दोनों धड़ों में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चुनाव आयोग पहुंच गई। एक धड़े के पास ज्यादातर विधायकों और सांसदों का समर्थन था तो दूसरे धड़े के पास संगठन का समर्थन था। इस स्थिति में आयोग ने चुनाव चिह्न और पार्टी का नाम दोनों फ्रीज कर दिया। 1989 के विधानसभा चुनाव में जानकी गुट को एआईएडीएमके(जेआर) तो जयललिता गुट को एआईएडीएमके (जेएल) नाम मिला। दोनों पार्टियां चुनाव लड़ीं। जयललिता धड़े को 21 फीसदी से ज्यादा वोट मिले। पार्टी 27 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं, जानकी गुट को महज नौ फीसदी वोट और दो सीटों से संतोष करना पड़ा।
राज्य में डीएमके की सरकार बनी और जयललिता नेता प्रतिपक्ष बनीं। इसके बाद तय हो गया था पार्टी और चुनाव निशान जयललिता धड़े के पास जा सकता है। हालांकि, चुनाव के बाद दोनों धड़ों का विलय हो गया और जयललिता पार्टी की नेता बनीं। पार्टी का चुनाव निशान भी उनके पास आया। विधानसभा चुनाव के महज कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य की 39 में से 38 सीटों पर एआईएडीएमके और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली। वहीं, सत्ताधारी डीएमके को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई।
उद्धव और आदित्य ठाकरे जिस तरह पूरा जोर संगठन को एकजुट करने में लगा रहे हैं। इससे उन्हें जयललिता की तरह ही पार्टी पर कब्जा बरकरार रखने की उम्मीद होगी। एक्सपर्ट कहत हैं कि ऐसा होने पर लड़ाई काफी लंबी चल सकती है। क्योंकि राज्य में फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं।
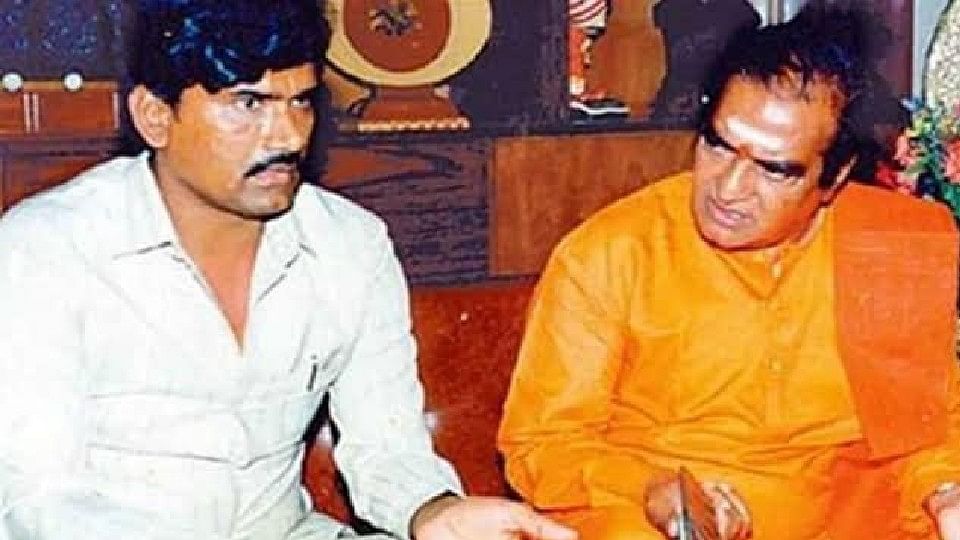
कौन से उदाहण हैं जिनसे बागी गुट का पलड़ा भारी है?
ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें बगावत होने पर पार्टी उस धड़े के पास गई जिसके पास ज्यादा विधायकों और सासंदों का समर्थन था। जैसे- 1969 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला गया तब उनके धड़े को कांग्रेस आर नाम मिला। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा की पार्टी को दो बैल की जगह गाय और बछड़ा चुनाव चिह्न मिला। बाद में इंदिरा का धड़ा ही असली कांग्रेस के रूप में स्थापित हुआ। इसी तरह 1995 में एन चन्द्रबाबू नायडू, 2016 में अखिलेश यादव की बगावत की। बगावत के वक्त इन लोगों के पास ज्यादातर विधायकों का समर्थन था। मामला चुनाव आयोग में जाने पर इन्हें ही पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न मिला।

शिवसेना किसके पास जाएगी?
संख्या बल की बात करें तो बागी गुट के पास विधायकों के साथ ज्यादातर सांसदों का भी समर्थन बताया जा रहा है। पार्टी पर दावे की लड़ाई अगर बढ़ती है तो मामला चुनाव आयोग भी जा सकता है। इस स्थिति में चुनाव आयोग तय करेगा की असली शिवसेना किसके पास है।
तीर-कमान चुनाव चिह्न किसके पास जाएगा?
अगर दोनों गुटों में समझौता नहीं होता है तो फैसला चुनाव आयोग से होगा। 1968 का इलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर चुनाव आयोग (ईसी) को किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर फैसला लेने की छूट देता है। चुनाव चिह्न किसे मिलेगा, इसका फैसला करने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है। यह भी हो सकता है कि चुनाव आयोग चुनाव चिह्न किसी को न दे।
इस नियम के मुताबिक, "चुनाव आयोग एक ही पार्टी में दो विपक्षी धड़ों की बात को पूरी तरह सुनेगा और सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगा। इसके अलावा ईसी दोनों धड़ों के प्रतिनिधियों को भी सुनेगा। जरूरत पड़ी तो आयोग तीसरे पक्ष को भी सुन सकता है और फिर चुनाव चिह्न किसी एक धड़े को देने या न देने से जुड़ा फैसला सुना सकता है।" इस नियम की सबसे खास बात यह है कि आयोग का फैसला सभी पक्षों के लिए सर्वमान्य होगा।

ये लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है?
पार्टी और उसके चुनाव चिह्न पर दावे की ये लड़ाई लंबी चल सकती है। इतिहास बताता है कि पार्टी किसकी इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हो ऐसा भी हो सकता है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव तक मामला खिंचता है तो चुनाव के दौरान दोनों धड़ों को अस्थाई नाम और चुनाव चिह्न मिल सकता है। इसके पुराने उदाहरण भी हैं।


